थार्नडाइक का बहु-कारक सिद्धान्त (Thorndike’s Multiple-Factor Theory)
बुद्धि के बहु-कारक सिद्धान्त का प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक (Edward Lee Thorndike-1874-1949. A.D.) ने सन् 1928 में किया था। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन (Spearman) के बुद्धि के द्वि-कारक सिद्धान्त का खण्डन करते हुए स्पष्ट किया था कि बुद्धि की संरचना बहुत से कारकों के योग से होती है। प्रत्येक कारक एक विशिष्ट मानसिक योग्यता (Specific Mental Ability) का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं का योग है। थॉर्नडाइक ने व्यक्ति के शारीरिक (Physical), सामाजिक (Social), क्रियात्मक (Conative), स्थानिक (Spatial), वाचिक (Speech) एवं सांख्यिक (Numerical) आदि योग्यताओं की पहचान कर प्रस्तुत किया था, जिन्हें व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करता है। थार्नडाइक के अनुसार, “बुद्धि अनेक जन्मजात योग्यताओं का मिश्रण है।”। (Intelligence consists of a number of innate abilities.)
इसे बुद्धि का बहु-कारक सिद्धान्त या असत्तात्मक सिद्धान्त (Multi-factor Theory or Anarchic Theory) भी कहते हैं। थार्नडाइक के अनुसार “बुद्धि विशिष्टीकृत और स्वतन्त्र मानसिक शक्तियों से निर्मित है।” (Intelligence is comprised of highly particularised and independent faculties.) उनके मध्य कोई महत्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं है। इस सिद्धान्त के अनुसार एक क्षेत्र में व्यक्ति के एक कार्य, करने की योग्यता से हम दूसरे प्रकार के कार्य में उसकी योग्यता के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं और ये अनेक योग्यताएँ एक-दूसरे से पूरी तरह स्वतन्त्र हैं। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि परीक्षाएँ समग्र बुद्धि का माप न करके केवल मात्र कुछ सामान्य योग्यताओं का ही माप करती हैं। थार्नडाइक के मत में बुद्धि में प्रमुख रूप से आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति, भाषा तथा भाषण योग्यता तथा दैशिक योग्यता का योगदान अधिक रहता है। इसके अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्व (G-factor) जैसी कोई चीज नहीं होती वरन् सभी कार्यों से कुछ समान तत्व होते हैं और इसी कारण अनेक परीक्षण प्राप्तांक में अनुबन्ध होता है। जब दो या अधिक परीक्षण प्राप्तांकों के मध्य उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध पाया जाता है तो इसका तात्पर्य है कि यह सह-सम्बन्ध किसी ऐसे सामान्य तत्व के कारण है जो सभी परीक्षणों में व्याप्त है। इस सामान्य तत्व की मात्रा सह-सम्बन्ध की मात्रा पर निर्भर करती है। सामान्य तत्व जितना अधिक होगा, उन सभी परीक्षणों में सह-सम्बन्ध भी उतना ही अधिक होगा।
इन्हीं तत्वों के आधार पर थार्नडाइक ने अमूर्त, मूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का अस्तित्व स्वीकार किया है।
Table of Contents
बहु-कारक सिद्धान्त की विशेषताएँ (Characteristics of Multi-factor Theory)
बहु-कारक सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-
1. इस सिद्धान्त के अनुसार सामान्य बुद्धि सदृश कोई चीज नहीं होती है।
2. बुद्धि कई विशेष मानसिक क्रियाओं/क्षमताओं का योग होती है।
3. इस सिद्धान्त के अनुसार अनुभवों के मध्य उद्दीपन अनुक्रिया का सम्बन्ध जितना अधिक होता है, भविष्य में उसी प्रकार के अनुभव समस्या समाधान में सहायक होते हैं और व्यक्ति उतना अधिक बुद्धिमान कहा जाता है।
बुद्धि के गुण (Attributes of Intelligence)
थार्नडाइक ने बुद्धि की चार विशेषताओं या गुणों को प्रस्तुत किया है, जो निम्न प्रकार हैं-
(1) स्तर (Level) – इसका अर्थ है किसी कार्य को सम्पादित करने में कठिनाई की सीमा। (Level refers to the degree of difficulty or a task that can be solved.) यह हमारी बुद्धि के स्तर को निर्धारित करता है। स्तर बुद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू है लेकिन हम इसका मापन अलग से नहीं कर सकते हैं।
(2) विस्तार (Range) – इसका अर्थ है कठिनाई के निश्चित स्तर पर अनेक कार्य जिन्हें हम सम्पादित कर सकते हैं। (Range or width refers to a number of tasks at any given degree of difficulty that we can solve.) बौद्धिक बुद्धि के विस्तार को केवल स्तर द्वारा नहीं बल्कि अनुभव के विस्तार और सीखने के अवसर द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों के समान कठिनाई की चीजों द्वारा विस्तार को प्रस्तुत किया जाता है।
(3) क्षेत्र (Area) – एक परीक्षण में क्षेत्र का अर्थ है प्रत्येक स्तर पर स्थितियों, की कुल संख्या जिनके प्रति अनुक्रिया करने में व्यक्ति समर्थ होता है। क्षेत्र व्यक्ति की बुद्धि के प्रत्येक स्तर पर सभी विस्तारों का कुल योग है। आमतौर पर उच्चता के साथ इसका सह-सम्बन्ध अधिक होता है। (Area is summation of all the ranges at each level of intelligence processed by an individual.)
(4) गति (Speed) – गति से हमारा अर्थ है वह रफ्तार या तेजी जिससे हम परीक्षण की मदों के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं। गति और उच्चता का सकारात्मक रूप से सह-सम्बन्ध होता है। इनका गुणांक 50 होता है। (By speed we mean rapidity with which we can respond to test items.)
प्रत्येक बुद्धि परीक्षण में ये चार विशेषताएँ निहित होती हैं। जब हम व्यक्ति का परीक्षण करते हैं तो हम उसे एक विशेष संख्या के कार्य देते हैं (क्षेत्र) और इन कार्यों की कठिनाई के स्तर (उच्चता) में अन्तर होता है और कठिनाई के प्रत्येक स्तर पर चीजों की एक विशिष्ट संख्या होती है (विस्तार) जिनके प्रति निर्धारित समय में अनुक्रिया की जाती है (गति)। इन विशेषताओं पर दिये गये बल में प्रत्येक परीक्षण के अनुसार अन्तर होता रहता है।
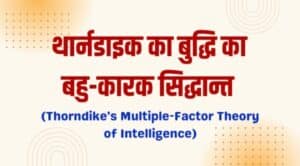
बुद्धि के प्रकार (Types of Intelligence)
थार्नडाइक ने बुद्धि के तीन प्रकार भी बताये हैं-
अमूर्त बुद्धि (Abstract Intelligence)
अमूर्त बुद्धि का अर्थ है- शब्दों, संख्याओं, अक्षरों, सम्प्रत्ययों, विचारों आदि के प्रति अनुक्रिया करने की योग्यता। इसमें अमूर्त विचारों, प्रतीकों, शब्दों, अंकों, सूत्रों और रेखाचित्रों के रूप में प्रस्तुत की गई समस्याओं का समाधान करने की योग्यता निहित है। (Abstract intelligence consists in ability to solve problems presented in form of abstract ideas, symbols, words, numbers, formulae and diagrams.) स्कूल में सभी शैक्षिक विषयों के लिये अमूर्त बुद्धि पूर्व शर्त है। जैसे-भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित दर्शनशास्त्र आदि। स्कूल मैं उच्च स्तर की सफलता अर्जित करने के लिये उच्च स्तर की अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है।
अमूर्त बुद्धि के तीन आयाम हैं-
(i) स्तर (Level) – कार्य का कठिनाई स्तर।
(ii) गति (Speed) – व्यक्ति के कार्य करने की गति।
(iii) प्रसार (Range) – कठिन कार्यों की संख्या, जिन्हें व्यक्ति कर पाता है।
मूर्त बुद्धि (Concrete Intelligence)
इसका तात्पर्य यांत्रिक या गामक (Motor) या मूर्त वस्तुओं से है अर्थात मूर्त पदार्थों या वस्तुओं के साथ अनुकूलन की योग्यता को मूर्त बुद्धि कहते हैं। इसमें कौशल-युक्त व्यवसायों और उपकरणों जैसी चीजों के साथ व्यवहार करने की योग्यता निहित है। (Concrete intelligence consists in ability to deal with things as in skilled trades and appliances.) बहुत से व्यक्ति बिना प्रशिक्षण के कई यंत्रों व मशीनों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं जबकि कुछ व्यक्तियों में यह क्षमता छोटे व स्थूल यंत्रों को भी ठीक करने की नहीं होती। व्यक्ति के जीवन की विभिन्न क्रियाओं में मूर्त बुद्धि का पता लगता है। इस प्रकार की बुद्धि को क्रिया परीक्षण (Performance Test) या चित्र परीक्षण (Picture Test) द्वारा मापा जा सकता है।
सामाजिक बुद्धि (Social Intelligence)
सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय है किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों से प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करने की क्षमता। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति की दैनिक जीवन की सामाजिक परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की योग्यता ही सामाजिक बुद्धि है। इसमें व्यक्ति अपने को समाज के अनुकूलन व्यवस्थित करने की क्षमता रखता है। सामाजिक बुद्धि का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग होता है। नेतृत्व, तार्किक शक्ति, सामाजिक कार्यों में रुचि, सामाजिक कल्याण की भावना, सहयोग की भावना आदि इस प्रकार की बद्धि के लक्षण हैं। जो व्यक्ति लोगों को अपनी कुशलता से प्रभावित करने की क्षमता रखता है उसमें उतनी ही अधिक सामाजिक बुद्धि व्यक्ति को जीवन में व्यवहारिक सफलता प्रदान करने में सहायता करती है।
थार्नडाइक के बुद्धि के सिद्धान्त के शैक्षिक निहितार्थ (Educational Implications of Thorndike’s Theory of Intelligence)
(1) बुद्धि के प्रकारों की जानकारी (Knowledge of Types of Intelligence)- थार्नडाइक का बुद्धि सिद्धान्त, बुद्धि के तीन प्रकारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है-
(i) अमूर्त बुद्धि, (ii) यान्त्रिक बुद्धि, (iii) सामाजिक बुद्धि
ताकि छात्रों को सही दिशा में निर्देशित किया जा सके। निर्देशन कार्यकर्ता द्वारा छात्र की योग्यताओं का विश्लेषण एक विश्वसनीय आधार प्रदान कर सकता है जिस पर भावी अधिगम का उपयोग किया जा सके।
(2) धीमी प्रगति के कारण (Causes of Slow Progress)- थार्नडाइक का बुद्धि सिद्धान्त छात्रों की पर्याप्त बुद्धि के बावजूद उनके असन्तोषजनक कार्य-प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने में उपयोगी होता है।
(3) पाठ्यक्रम में निहितार्थ (Implications in Curriculum)- थार्नडाइक के बुद्धि सिद्धान्त के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि के विकास के लिए अवसर प्रदान करे। आधुनिक स्कूल पाठ्यक्रम को विविधता प्रदान कर दी गई है और उसका आधार विस्तृत कर दिया गया है। (Modern school curriculum has been diversified and broad-based.)
(4) शिक्षण विधियों में निहितार्थ (Implications in Methods of Teaching)- शिक्षण की आधुनिक तकनीकी के उपयोग द्वारा छात्रों की अमूर्त, यान्त्रिक और सामाजिक योग्यताओं का विकास होता है।
(5) ध्यान का केन्द्र (Focus of Attention)- थार्नडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि का प्रतिपादन किया है, इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हम उनमें से प्रत्येक पर उचित ध्यान दे रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है। अमूर्त, यान्त्रिक और सामाजिक बुद्धि के विकास तथा अमूर्त, यान्त्रिक एवं सामाजिक कौशलों के विकास पर हमारा ध्यान केन्द्रित होना चाहिए।
(6) संवर्द्धन कार्यक्रम (Enrichment Programme) – थार्नडाइक का सिद्धान्त प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और पिछड़े हुए छात्रों के लिए संवर्द्धन कार्यक्रमों को तैयार करने में अध्यापकों को निर्देशन देता है। यह सिद्धान्त विद्यालय की कार्यविधि के लिए नये विचारों का सुझाव देता है।
(7) उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching)- जब अमूर्त, यान्त्रिक और सामाजिक बुद्धि वाले कुछ छात्र सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रभावशाली रूप से सीखने में असफल रहते हैं तो इस स्थिति में सुधारात्मक या उपचारात्मक शिक्षण के लिए उनकी योग्यताओं का सही-सही मूल्यांकन किये जाने की ओर जहाँ पर वे कमजोर हैं, वहाँ उसकी क्षमताओं का उनके द्वारा उपयोग किये जाने और विकसित किये जाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता होती है।
(8) भावी अधिगम का आधार (Basis of Future Learning)- बुद्धि के यान्त्रिक और सामाजिक पहलू विभिन्न विशिष्टीकरण प्रक्रियाओं (शैक्षिक और व्यावसायिक) में शामिल रहते हैं। इसलिए छात्र को सही दिशा में डालने के लिए हमें प्रत्येक छात्र की विशिष्ट प्रकार की बुद्धि के बारे में पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति की जानकारी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है।
(9) निर्देशन का आधार (Basis of Guidance)- अमूर्त, यान्त्रिक और सामाजिक बुद्धि की जानकारी छात्र को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने का आधार प्रदान करती है।
